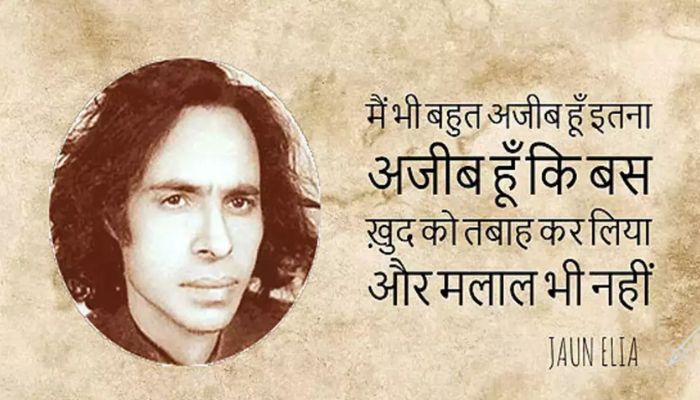Gender Equality : लैंगिक समता के मामले में भारत 146 देशों में से 135 वें पायदान पर है। हद तो यह है कि दक्षिण एशिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही हमसे पीछे हैं। रिपोर्ट की समता सूची बताती है कि हम बांग्लादेश से 60 पायदान पीछे हैं, जबकि नेपाल से 39, श्रीलंका से 25, मालदीव से 18 और भूटान से 9 पायदान पीछे हैं। महिला स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा के लिहाज से तो हमारी स्थिति एकदम गई-गुजरी है।
Gender Equality:
पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्पन्न एक विवाह परिचय सम्मेलन में जाना हुआ। इस सम्मेलन में तकरीबन 400 परिवार एक-दूसरे से मिले और एक-दूसरे को जाना। इस सम्मेलन में एक बात जो उभरकर सामने आयी, वह यह थी कि करीब 80 फीसदी परिवार ऐसे थे, जिन्हें उच्चशिक्षित बहू तो चाहिए थी, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि बहु नौकरी नहीं करेगी। हो सकता है, कहने-सुनने में ये छोटी-सी बात लगे, लेकिन यह बात वास्तव में समाज की सोच का एक बड़ा नमूना है। एक ऐसा नमूना, जो हमें आईना दिखाता है, जो हमें बताता है कि महिलाओं को लेकर हमारी सोच में आजादी के 75 सालों बाद भी कोई खास बदलाव नहीं आया।
हैरानी की बात तो यह है कि देश की सबसे विश्वस्त संस्था ‘सेना’ की भी कमोवेश यही सोच है। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को दिये अपने फैसले में सेना से अपना घर दुरुस्त करने को कहा है। वास्तव में यह फैसला उन 34 महिला सैन्य अधिकारियों से जुड़ा है, जिन्होंने याचिका दायर करके सेना पर यह आरोप लगाया था कि लड़ाकू और कमांडिंग भूमिकाओं से जुड़े प्रमोशन में उनकी अनदेखी की जा रही है। उनके बजाय जूनियर पुरुष अफसरों को प्रमोशन दिया जा रहा है। याचिका दायर करने वाली सैन्य अधिकारियों में कमांडर रैंक की दो अधिकारी शामिल हैं। ये सिर्फ प्रमोशन में अनदेखी करने भर का मामला नहीं है। महिला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2020 के आदेश के बाद सेना ने स्थायी कमीशन दिया। इससे पहले वे सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अधिकतम 14 साल तक ही अपनी सेवाएं दे सकती थीं। महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए लंबी लड़ाई लडऩी पड़ी और अब पदोन्नति के लिए फिर वही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इन अधिकारियों का आरोप है कि स्थायी कमीशन मिलने से अब तक तकरीबन 1200 जूनियर पुरुष अधिकारियों को प्रमोशन दिया जा चुका है, लेकिन उनकी लगातार अनदेखी हो रही है। अगर वरिष्ठ पदों पर महिलाओं के साथ इस तरह भेदभाव हो रहा है तो इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि निचले पायदान की महिला सैन्य कर्मी इससे कहीं अधिक भेदभाव की शिकार हैं।
इस बात को देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था संसद में भी महिलाओं की स्थिति से समझा जा सकता है। संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का मामला ढाई दशक से भी ज्यादा समय से अलग-अलग वजहों के चलते अटका हुआ है। संसद में 15वीं लोकसभा के दौरान 9 मार्च 2010 में महिलाओं को आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव लाया गया तो उस समय लोकसभा में कई नेताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। जिस वजह से यह पास नहीं हो सका। इसके बाद कई बार इसके लिए संसद में आह्वïान हुए। महिलाओं के पक्ष में बड़ी-बड़ी बातें की गईं, लेकिन आज तक यह बिल पास नहीं हुआ और बहुत कम संभावना है कि मौजूदा 17वीं लोकसभा में भी यह प्रस्ताव पास हो जाए, क्योंकि लोकसभा के पांच साल के कार्यकाल के बाद अगर कोई बिल पास नहीं होता तो वह स्वत: रद्द हो जाता है। उसे पास कराने के लिए फिर नये सिरे से सदन में पेश करना होता है। कम ही उम्मीद है कि बार-बार इस बिल को संसद में पेश करने की कोई जहमत उठायेगा और इसे सांसद पास कर देंगे। यह उम्मीद इसलिए कम है, क्योंकि पार्टियां भले वह कोई हो, संसद में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद चुनकर आयी थीं, जो अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा थीं। हां, राज्यसभा और लोकसभा की महिला सांसदों को एक कर दिया जाए तो यह पहला ऐसा मौका है जब उनकी संख्या 100 से ज्यादा है। लेकिन औसत के हिसाब से दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारतीय संसद में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है।
स्थानीय निकायों में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, क्योंकि वहां 33 फीसदी का आरक्षण है, जिस कारण देश की पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 9 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं और तिहरे स्तर वाली पंचायत प्रणाली में 59 हजार से अधिक महिला अध्यक्ष हैं। ऐसा इसलिए संभव हुआ, क्योंकि यहां महिलाओं के लिए आरक्षण है। यह आरक्षण पहले 33 फीसदी था, मगर अब 28 में से 21 राज्यों में यह 33 से बढक़र 50 फीसदी हो गया है। सवाल है, नीति निमार्ताओं की संस्था लोकसभा में महिलाएं क्यों 33 फीसदी नहीं हैं?
वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से पेश वैश्विक लैंगिक भेदभाव रिपोर्ट-2022 भी इस बात की चुगली करती है कि भारतीय समाज में अभी जबरदस्त पुरुषवादी सोच हावी है। लैंगिक समता के मामले में भारत 146 देशों में से 135 वें पायदान पर है। हद तो यह है कि दक्षिण एशिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही हमसे पीछे हैं। रिपोर्ट की समता सूची बताती है कि हम बांग्लादेश से 60 पायदान पीछे हैं, जबकि नेपाल से 39, श्रीलंका से 25, मालदीव से 18 और भूटान से 9 पायदान पीछे हैं। महिला स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा के लिहाज से तो हमारी स्थिति एकदम गई-गुजरी है। इस कसौटी में भारत 146 देशों में सबसे पीछे है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान आंकड़ों को देखते हुए भारत में लैंगिक भेदभाव की खाई पाटने के लिए 132 साल लग जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि महिला सांसदों, विधायकों, प्रबंधकों और वरिष्ठ अधिकारियों की हिस्सेदारी पिछले एक साल में 14.6 फीसदी से बढक़र 17.6 फीसदी हो गई है। लेकिन सवाल है, क्या ये संतोषजनक है? आर्थिक विशेषज्ञों का आकलन बताता है कि कोरोना काल में 40 फीसदी महिलाओं को छंटनी के नाम पर नौकरी से हाथ धोना पड़ा और बाद में इन महिलाओं में से सिर्फ 7 फीसदी ही दोबारा से जॉब हासिल कर पायी। मतलब, कोरोना ने 33 फीसदी महिलाओं का रोजगार छीन लिया और वे घर की चाहरदीवारी में कैद होकर रह गई।
वैसे, साल-2022 के जाते-जाते कुछ सुखद खबरें भी आयी हैं। मसलन, उत्तर प्रदेश के मिजापुर जिले के छोटे से गांव जसोवर की सानिया मिर्जा का एनडीए में फाइटर पायलट की ट्रेनिंग के लिए चयन हुआ है। सानिया मुस्लिम समाज की पहली ऐसी लडक़ी हैं, जो फाइटर जेट उड़ाएंगी। पेशे से टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी सानिया की प्रेरणा स्रोत हैं, देश की पहली महिला फाइटर अवनी चतुर्वेदी। सानिया ने यह उपलब्धि यूपी बोर्ड से पढक़र हासिल की है, जिससे उनकी मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकता है।
इसी तरह, प्रियंका शर्मा यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बनी हैं। इससेपहले उन्होंने ट्रक ड्राइवर का भी काम किया है। उधर, सेना की कैप्टन शिवा चौहान ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वे दुनिया की सबसे ऊंची युद्घभूमि सियाचीन में तैनात होने वाली पहली महिला अफसर बन गई हैं। ये उपलब्धिपूर्ण खबरें उम्मीदें तो जगाती हैं लेकिन महिलाओं की कामयाबी की रफ्तार में समाज की सोच आडे आ ही जाती है। इस सोच को बदलने की जरूरत है ताकि लैंगिक भेदभाव को जल्द से जल्द जड़ से मिटाया जा सके।